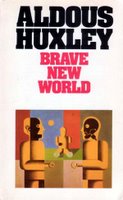Posted by Ankit On August 24th, 2006
आज जब जà¥à¤¦à¤¾ होने की बात आई,
यह समां इतना रंगीन कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ हो गया,
मेरा महबूब कà¥à¤› ज़à¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ हसीन कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ हो गया है ।
पानी पे चाà¤à¤¦ इतना खà¥à¤¶ कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ लग रहा है,
बीता हà¥à¤† वक़à¥à¤¤ आज इतना कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ सà¥à¤²à¤— रहा है ।
हवाओं की ठणà¥à¤¡à¥€ थपकी में आज यह नरमी कैसी ?
रात की कोमल रोशनी में à¤à¤²à¤¾ यह गरमी कैसी?
और तà¥à¤®à¥à¤¹à¤¾à¤°à¥‡ बारे में कà¥à¤¯à¤¾ कहूं ?
"रंगो, छंदों में समायेगी, किस तरह से इतनी सà¥à¤‚दरता ?"
आज इन आà¤à¤–ों में चांद की शरारत चमक रही है
जैसे कि कितने सारे राज़ इनकी गहराईयों से बाहर आने को बेताब हों
कितने सारे सवाल, कितने सारे किसà¥à¤¸à¥‡ इसकी गरà¥à¤¤ में दफ़à¥à¤¨
दिल को कितना ज़à¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ à¤à¥‡à¤¦ रहीं हैं यह आज
जैसे ना चाहते हà¥à¤¯à¥‡ à¤à¥€ बीते हà¥à¤¯à¥‡ खà¥à¤¶à¤—वांर वकà¥à¤¤ की दà¥à¤¹à¤¾à¤ˆ दे रहीं हों
और इन होठों पे à¤à¤• अनसà¥à¤¨à¥€, अनकही दासà¥à¤¤à¤¾à¤ है
मà¥à¤¸à¥à¤•à¥à¤°à¤¾à¤¹à¤Ÿ इनकी कैद से रहरहकर बाहर à¤à¤¾à¤à¤• रही है,
जैसे à¤à¤• डगमगाते हà¥à¤¯à¥‡, à¤à¤°à¥‡ हà¥à¤¯à¥‡ पैमाने से मै की दो बूंदे गिरने को बेताब हों
इन अधखà¥à¤²à¥‡ होठों पर इतना निमंतà¥à¤°à¤£ कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ है ?
इस दिल में बेवजह ही इतना कंपन कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ है ?
इन आà¤à¤–ों के तीर मेरे दिल के पार हो रहे
मेरे सारे हौसले तेरे सामने बेकार हो रहे !
लेकिन ना जानते हà¥à¤¯à¥‡ à¤à¥€ कितनी सà¥à¤µà¤¾à¤°à¥à¤¥à¥€ हो गयी हो तà¥à¤®
तà¥à¤®à¥à¤¹à¤¾à¤°à¥‡ इस रूप ने इस कातिलाना मंज़र के साथ मिलके मेरे मन में हज़ार सवाल पैदा कर दिये हैं
इस जà¥à¤¦à¤¾à¤ˆ की सारà¥à¤¥à¤•à¤¤à¤¾ के बारे में सोचने लग गया हूं।
तà¥à¤®à¥à¤¹à¤¾à¤°à¥‡ बगैर इस सफर की असहनीयता के बारे में सोचने लगा हूं
मैं कितना कमज़ोर, कितना बेचारा और तà¥à¤® कितनी निषà¥à¤ à¥à¤°, कितनी दूर ।
"इस पार पà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‡, मधॠहै तà¥à¤® हो, उस पार न जाने कà¥à¤¯à¤¾ होगा
दà¥à¤°à¤— देख जहाठतक पाते हैं, तम का सागर लहराता है
फिर à¤à¥€ उस पार खड़ा कोई, हम सबको खींच बà¥à¤²à¤¾à¤¤à¤¾ है
मैं आज चला तà¥à¤® आओगी, कल, परसों, सब संगी साथी
दà¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है
मेरा तो होता मन डगमग, तट पर ही के हलकोरों से
जब मैं à¤à¤•à¤¾à¤•à¥€ पहà¥à¤‚चूंगा, मà¤à¤§à¤¾à¤° न जाने कà¥à¤¯à¤¾ होगा
इस पार पà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‡, मधॠहै तà¥à¤® हो, उस पार न जाने कà¥à¤¯à¤¾ होगा"